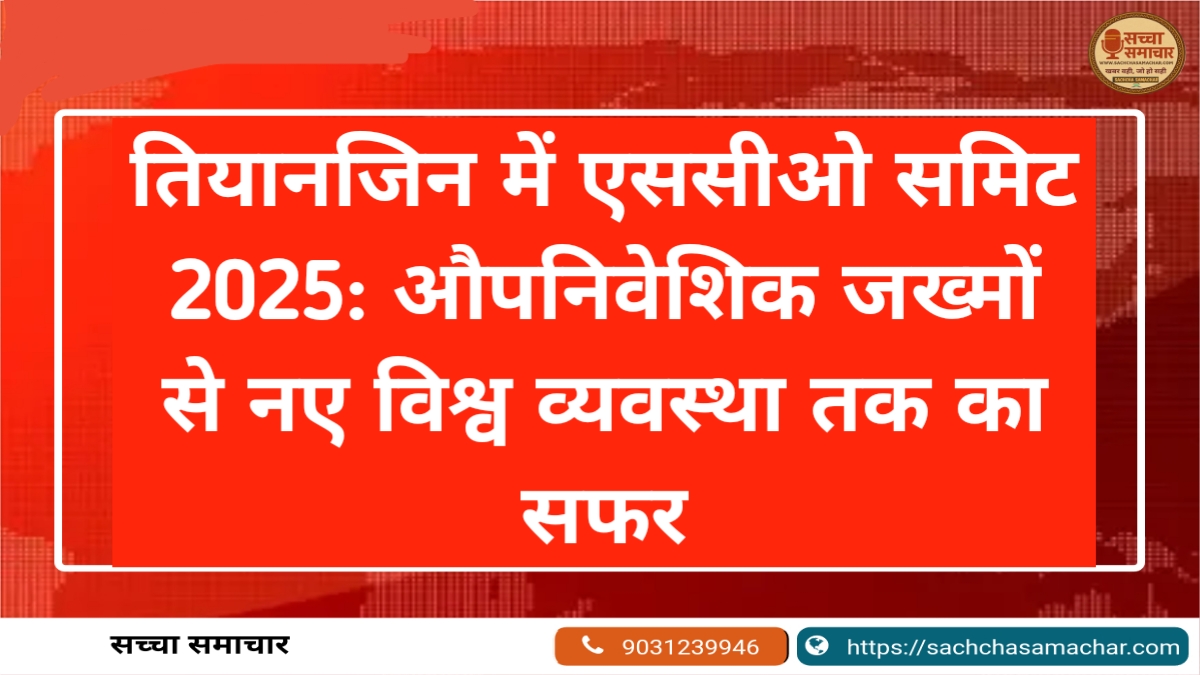अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कुछ फैसले ऐसे होते हैं, जो सिर्फ आज के समीकरण नहीं, बल्कि आने वाले कई सालों की ग्लोबल पॉलिटिक्स की दिशा तय कर देते हैं। हाल ही में अमेरिका ने फिर से कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं, जिसने बड़ी बहस छेड़ दी है: क्या दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अब अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में सिर्फ अपने फायदे के लिए रहेगी, या सबको साथ लेकर चलेगी?
अमेरिकी प्रशासन ने अपने दूसरे कार्यकाल में आते ही एक बड़ी समीक्षा शुरू की— खासकर विदेशी सहायता और उन अंतरराष्ट्रीय संगठनों पर, जहाँ अमेरिका अपना पैसा और डिप्लोमेटिक ताकत लगा रहा है। उनका सीधा संदेश था कि अब हमें यह देखना होगा कि जिन संस्थानों को हम इतना कुछ दे रहे हैं, क्या वे वाकई हमारे राष्ट्रीय हितों और हमारे “अमेरिका फर्स्ट” एजेंडे के साथ तालमेल बिठा रहे हैं?
इसी समीक्षा का सीधा नतीजा है— अमेरिका ने UNESCO (यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गनाइजेशन) से अपनी वापसी का ऐलान कर दिया।
’अमेरिका फर्स्ट’ का ग्लोबल चश्मा
”अमेरिका फर्स्ट” का नारा चुनावी रैलियों से शुरू हुआ था, और इसका मतलब साफ़ था: अमेरिकी नीतियाँ, फैसले और संसाधन सबसे पहले अमेरिकी जनता के लिए इस्तेमाल होंगे।
इस एजेंडे के तहत, प्रशासन ने कई बार साफ़ किया कि अगर कोई अंतरराष्ट्रीय मंच या संगठन अमेरिकी मूल्यों, हितों, या रणनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है, तो अमेरिका उसका हिस्सा नहीं रहेगा। यही वजह है कि पहले विदेशी सहायता पर कैंची चली, और अब अंतरराष्ट्रीय संगठनों पर ध्यान गया। सवाल यह नहीं था कि हम कितना पैसा दे रहे हैं, सवाल यह था कि क्या यह निवेश हमारे लिए सच में फायदेमंद है?
यूनेस्को पर उंगली क्यों?
UNESCO की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका काम था शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान के जरिए दुनिया में शांति और समझदारी बढ़ाना। ताजमहल से लेकर मिस्र के पिरामिड तक, दुनिया की कई धरोहरें इसी की वजह से वैश्विक पहचान पाती हैं।
लेकिन अमेरिका का आरोप यह रहा कि समय के साथ यह संगठन “राजनीतिक रंग” में रंग गया। अमेरिका की मुख्य आपत्ति यह थी:
- इजरायल पर पक्षपात: अमेरिकी विदेश विभाग ने साफ कहा कि UNESCO में इजरायल से जुड़े मुद्दों पर निष्पक्षता नहीं रहती।
- मूल्यों का टकराव: संगठन के कुछ फैसलों और नीतियों को “अमेरिका फर्स्ट” एजेंडा और अमेरिकी मूल्यों के खिलाफ माना गया।
- विवादित स्थलों पर फैसला: अरब देशों और इजरायल के बीच के विवादित स्थलों को लेकर लिए गए फैसलों में अमेरिका को पक्षपात दिखा।
इन्हीं कारणों के चलते अमेरिका ने कह दिया, “बस, अब हम इस संगठन का हिस्सा नहीं रहेंगे।”
दुनिया का रिएक्शन और बड़ा सवाल
अमेरिका के इस कदम से दुनिया दो धड़ों में बंट गई। इजरायल ने तुरंत इस फैसले का स्वागत किया। वहीं, यूरोपीय देशों और संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के हटने से UNESCO कमजोर होगा।
तो क्या यह अमेरिका के लिए सही कदम है?
एक पक्ष मानता है कि अमेरिका सही है। अगर कोई संगठन बार-बार आपके खिलाफ पक्षपात कर रहा है और आपका भारी निवेश बेकार जा रहा है, तो ऐसी सदस्यता क्यों जारी रखी जाए? यह संसाधनों की बर्बादी ही है।
दूसरा पक्ष कहता है कि अमेरिका ने गलती की। जब आप वैश्विक मंचों से हटते हैं, तो वैश्विक नेतृत्व की आपकी छवि कमजोर होती है। आप पीछे हटते हैं, तो चीन और रूस जैसे देशों को आगे आने का मौका मिल जाता है—जोकि अमेरिका के दीर्घकालिक हित में नहीं है।
भविष्य की तरफ इशारा
UNESCO से वापसी सिर्फ एक संगठन से दूरी नहीं है। यह आने वाले समय की वैश्विक राजनीति का संकेत है:
- अन्य संगठनों पर खतरा: अमेरिका ने इशारा दिया है कि UNESCO पहला है, आखिरी नहीं। WHO, WTO और दूसरे संस्थानों पर भी समीक्षा की तलवार लटकी है।
- ताकत का संतुलन: अमेरिका के हटने से जो खाली जगह बनती है, उसे भरने के लिए चीन और रूस अपनी कूटनीतिक पकड़ मजबूत करेंगे।
- भारत और अन्य देशों के लिए मौका: अमेरिका की गैरमौजूदगी में भारत जैसे देशों के पास मौका है कि वे इन वैश्विक मंचों पर अपनी भूमिका और प्रभाव को और बढ़ाएं।
निष्कर्ष: सहयोग या स्वार्थ?
अमेरिका की UNESCO से वापसी एक साफ संकेत है: आने वाले वर्षों में अमेरिका हर अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को सिर्फ अपने हित के चश्मे से देखेगा।
यह नीति एक ओर जहां अमेरिकी हितों की सुरक्षा करती है, वहीं दूसरी ओर बहुपक्षीय संस्थाओं (multilateral institutions) की नींव कमजोर करती है।
अब दुनिया को यह तय करना होगा कि क्या हम सिर्फ अपने-अपने राष्ट्रीय हितों के लिए वैश्विक मंचों से जुड़ेंगे, या फिर मिलकर एक साझा भविष्य का निर्माण करेंगे। यह सवाल ही आज की अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है।
आपको क्या लगता है, अमेरिका का यह कदम उसके लिए फायदेमंद साबित होगा, या वैश्विक नेतृत्व के लिए महंगा पड़ेगा?